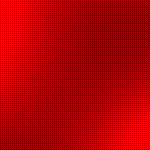हम भारत में जरूरत की केवल 20 प्रतिशत अदालतों से देश में न्यायालयों की कमी ने अनेक समस्याएँ खड़ी की हैं और लगातार हो रही हैं। अदालतों की इस कमी ने सब से बड़ी समस्या खड़ी की है कि मुकदमों के निर्णय में असीमित देरी होती है जिस के कारण न्याय का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जा रहा है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिन का निर्णय जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसे जिन का निर्णय होने की कोई समय सीमा ही नहीं है। न्यायार्थी के जीवन में यदि निर्णय हो भी जाए तो वह खुद को खुशकिस्मत समझता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली ने न्यायपालिका को कम धन आंवटन पर सवाल उठाया है कि नौवीं योजना में सरकार ने न्यायिक प्रणाली के लिए सिर्फ 385 करोड़ रुपये आवंटित किए जो खर्च योजना का सिर्फ 0.071 फीसदी था। दसवीं योजना में स्थिति में आंशिक रूप से सुधार आया जब सरकार ने 700 करोड़ या खर्च योजना का 0.078 फीसदी खर्च किया। इस सवाल से स्पष्ट है कि हमारी सरकार का ध्यान न्यायव्यवस्था को आवश्यकता के अनुसार विकसित करने पर नहीं है, अपितु इसे वह अनावश्यक बोझ समझती है। वह देश और समाज में न्याय स्थापित करने के स्थान पर अन्य इतर उपायों से काम चलाना चाहती है।
ये इतर उपाय एक ओर तो लोक अदालतों में समझाइश से समझौते के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करने के रूप में सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर अर्ध न्यायिक संस्थानों की स्थापना कर उन्हें सीधे सरकार के अधीन कर देने के रूप में। लेकिन दोनों ही मार्ग वास्तविक न्याय से पलायन को प्रदर्शित करते हैं। हम फिलहाल लोक अदालतों और समझौतों की बात करें। लोक अदालतों में जज अपने निर्धारित स्थान से नीचे उतर कर एक हॉल में बैठता है। वहाँ पक्षकार भी समान स्तर पर बात करता है। लेकिन हमेशा कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर न्याय मांगने वाले पक्ष को समझाया जाता है कि मुकदमा लड़ने में कोई लाभ नहीं है, बहुतेरा पैसा और समय जाया होगा, आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। इस लिए अपने अधिकारों को छोड़ कर वह समझौता क्यों न कर ले। पूरी नहीं तो चौथाई रोटी तो मिल ही रही है। लोक अदालत में ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि न्यायार्थी को लगने लगता है कि उस ने न्याय के लिए अदालत आ कर गलती कर दी। वैसी अवस्था में या तो वह अपने अधिकारों को छो़ड़ कर समझौता कर लेता है या फिर अपनी लड़ाई को छोड़ बैठता है।
लेकिन क्या एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए समझौतों और लोक अदालतों की यह प्रक्रिया उचित है? मेरी राय में नहीं। इस से हम एक न्यापूर्ण समाज की ओर नहीं जा रहे हैं, अपितु अन्याय करने वालों को एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वैसी ही जैसे किसी को एक झापड़ कस दिया जाए और फिर माफी मांग ली जाए। फिर भी नाराजगी दूर न होने पर कहा जाए कि बेचारे ने माफी तो मांग ली अब क्या एक झापड़ के लिए उस की जान लोगे क्या।
ये इतर उपाय एक ओर तो लोक अदालतों में समझाइश से समझौते के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करने के रूप में सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर अर्ध न्यायिक संस्थानों की स्थापना कर उन्हें सीधे सरकार के अधीन कर देने के रूप में। लेकिन दोनों ही मार्ग वास्तविक न्याय से पलायन को प्रदर्शित करते हैं। हम फिलहाल लोक अदालतों और समझौतों की बात करें। लोक अदालतों में जज अपने निर्धारित स्थान से नीचे उतर कर एक हॉल में बैठता है। वहाँ पक्षकार भी समान स्तर पर बात करता है। लेकिन हमेशा कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर न्याय मांगने वाले पक्ष को समझाया जाता है कि मुकदमा लड़ने में कोई लाभ नहीं है, बहुतेरा पैसा और समय जाया होगा, आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। इस लिए अपने अधिकारों को छोड़ कर वह समझौता क्यों न कर ले। पूरी नहीं तो चौथाई रोटी तो मिल ही रही है। लोक अदालत में ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि न्यायार्थी को लगने लगता है कि उस ने न्याय के लिए अदालत आ कर गलती कर दी। वैसी अवस्था में या तो वह अपने अधिकारों को छो़ड़ कर समझौता कर लेता है या फिर अपनी लड़ाई को छोड़ बैठता है।
लेकिन क्या एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए समझौतों और लोक अदालतों की यह प्रक्रिया उचित है? मेरी राय में नहीं। इस से हम एक न्यापूर्ण समाज की ओर नहीं जा रहे हैं, अपितु अन्याय करने वालों को एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वैसी ही जैसे किसी को एक झापड़ कस दिया जाए और फिर माफी मांग ली जाए। फिर भी नाराजगी दूर न होने पर कहा जाए कि बेचारे ने माफी तो मांग ली अब क्या एक झापड़ के लिए उस की जान लोगे क्या।